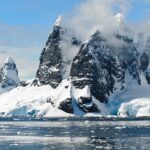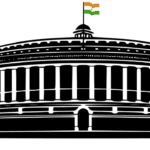जलवायु क्या है
जलवायु मौसम के औसत दशा को कहते है| अर्थात किसी स्थान के किसी निश्चित समय पर वायुमंडल की वार्षिक दशा और औसत परिणाम को जलवायु कहते है| इस तरह सालभर की दशा को जलवायु कहते है|
जलवायु के मूल तत्व
वायुमंडलीय ताप, आर्द्रता, वायुदाब, पवन की दिशा तथा वर्षा जलवायु के मूल तत्व है| जलवायु के तत्वों का महत्त्व सापेक्ष है| सभी तत्व महत्वपूर्ण है| वायुमंडल के सभी किर्याओ की जड़ में उर्जा है| जो पृथ्वी की माध्यम से हवा मिलती है| जो जलवायु सम्बन्धी सभी प्रक्रियाओ का कारक बनती है|
जलवायु से सम्बंधित कुछ मापने वाला यंत्र
तापमान – थर्मामीटर thermometer
वायुदाब – बैरोमीटर barometer
पवन की दिशा – विंड-वैन vind-vane
पवन की गति – एनीमोमीटर anemometer
वायु की आर्द्रता – हाइग्रोमीटर hygrometer
वर्षा मात्रा मापी – रेन गेज rain guage
यहाँ पढ़े महाद्वीप और महासागर के नाम
भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक
किसी स्थान की जलवायु तत्वों पर निर्भर करती है| इन तत्वों में अक्षांश, ऊँचाई, समुद्र से निकटता, पवन की दिशा, वन, समुद्री जलधाराएँ, वर्षा, पर्वत, मिटटी और पृथ्वी की ढाल आदि शामिल है|
भारत की जलवायु कैसी है
भारत के जलवायु की विविध दशाएँ पायी जाती है| एक स्थान से दुसरे स्थान में और एक ऋतू से दुसरे ऋतू में तापमान और वर्षा में भारी अंतर है| भारत में मानसूनी जलवायु पायी जाती है| भारत मानसून पवनो के प्रभाव क्षेत्र में आता है|
भारत की जलवायु मानसूनी क्यों है
लगभग सम्पूर्ण देश में मानसून पवनो का इतना स्पष्ट प्रभाव पड़ता है कि यहाँ चार प्रमुख ऋतूएँ वर्ष भर में परिवर्तित होकर पायी जाती है| मानसून पवनो द्वारा समय-समय पर अपनी दिशा बिलकुल बदल देने के कारण ये ऋतूएँ भी क्रमानुसार चक्र की तरह बदलती रहती है|
भारत की जलवायु ऋतु
भारत में मिलने वाली चार प्रमुख ऋतू निम्नलिखित है
शीत ऋतू – दिसम्बर से मार्च तक
ग्रीष्म ऋतू – 10 मार्च से 20 जून तक
वर्षा ऋतू – 16 जून से 15 सितम्बर तक
शरद ऋतू – 16 सितम्बर से 15 दिसम्बर तक
मानसून पवनो के आगमन में होनेवाला विलम्ब इनको पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है|
भारत की जलवायु शीत ऋतु
भारत में दिसम्बर से मार्च तक का समय शीत ऋतू के अंतर्गत आता है| इस समय देश के अधिकांश भागो में महाद्वीपीय पवनें चलती है| इस ऋतू में उतरी मैदान में उच्च दाब होता है और समुद्र में निम्न वायुदाब |
इस समय उतर भारत में कम तापमान पाया जाता है| जैसे-जैसे उतर से दक्षिण की और बढ़ते जाओगे वहाँ सागरीय समीपता एवं उष्णकटिबंधीय स्थिति के करण तापमान बढ़ता जाता है|
उतर के विशाल मैदान में यह 10 डिग्री से 15 डिग्री तक पाया जाता है| पश्चिमी राजस्थान में तो रात के समय तापमान हिमांक बिंदु अथवा 10 डिग्री से निचे चला जाता है| इस काल में जम्मू-कश्मीर, पश्चिम पंजाब एवं राजस्थान में कुछ वर्षा भी होती है|
इस ऋतू में तमिलनाडू के कारोमंडल तट पर भी कुछ वर्षा होती है| इस काल में होनेवाली वर्षा देश की कुल औसत वर्षा का लगभग 2% ही होती है|
भारत की जलवायु ग्रीष्म ऋतु
भारत में 15 मार्च से 15 जून तक ग्रीष्म ऋतू मानी जाती है| मार्च के महीने में सबसे अधिक तापमान दक्कन के पठार में मिलता है जो अधिकतम 38 डिग्री तक रहता है| अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में तापमान सर्वाधिक 42 से 43 डिग्री हो जाता है|
मई में देश के उतरी-पश्चिम भाग में तापमान 40 डिग्री तक चला जाता है| इस समय इस भाग में गर्म हवाएँ चलने लगती है| इन्हें “लू” कहते है|
मई के महीने में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उतर प्रदेश में संध्या के समय धुल भरी आँधी चलने लगती है| कभी कभी आँधी के बाद हल्की वर्षा होने लगती है|
ग्रीष्म ऋतू में केरल तथा कुछ तटीय मैदानी भागो में कुछ वर्षा होती है| जिसे आम्रवृष्टि कहते है इसके अतरिक्त असम तथा पश्चिम बंगाल में भी तेज़ आर्द हवाएँ चलने लगती है| इन हवाओ को “काल वैशाखी” के नाम से जाना जाता है|
भारत की जलवायु वर्षा ऋतु
भारत में वर्षा ऋतू 15 जुलाई से 15 सितम्बर तक हमारे देश में वर्षा की ऋतू होती है| वर्षा ऋतू का समय दक्षिण से उतर तथा पूर्व से पश्चिम की और घटती जाती है| देश की सबसे उतरी-पश्चिमी भाग में यह समय दो महीने की होती है| इस अवधि में कुल वर्षा के तीन-चौथाई से लेकर, दस से नौ भाग तक होती है
दक्षिण-पश्चिम मानसून पवनें जब स्थलीय भागो में प्रवेश करती है तथा प्रचण्ड गर्जन एवं तडित के साथ के साथ तेज एवं घनघोर वर्षा करती है| इस प्रकार की पवनों के आगमन एवं उनसे होनेवाली वर्षा को “मानसून का फटना या टूटना” कहते है
ये पवनें प्रायदीप की उपस्थिति के कारण दो भागो में बाँट जाती है| बंगाल की खाड़ी का मानसून और अरब सागर का मानसून|
अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकाल में दक्षिण-पश्चिम मानसून से होती है| वर्षा जून से सितम्बर तक खूब होती है| वर्षा वाणिज्य पवन द्वारा होती है| वर्षभर में औसतन 150 से.मी से 200 से.मी के बीच वर्षा होती है| संसार में सर्वाधिक वर्षा मेघालय के चेरापूँजी तथा मासिन राम नामक स्थानों पर होती है|
शरद ऋतू
भारत में 16 सितम्बर से 15 दिसम्बर तक शरद ऋतू पायी जाती है| अक्टूबर के अन्त तक वर्षा की तीव्रता प्रायः कम हो जाती है| धीरे-धीरे दक्षिणी-पश्चिमी मानसून पीछे हटते हुए मध्य मध्य सितम्बर तक पंजाब, तथा अक्टूबर के अन्त तक गंगा का डेल्टा क्षेत्र तथा नवम्बर के प्रारम्भ में दक्षिण भारत को भी छोड़ देता है|
इस स्थिति के पश्चात उतर भारत में तापमान तेजी से घटता है| तथा दिसम्बर तक सूर्य के दक्षिणयन होने के कारण शीत ऋतू का आगमन हो जाता है| इस ऋतू में लौटती हुई मानसून के बंगाल की खाड़ी से गुजरने के कारण उसमे कुछ आर्द्रता आ जाती है और जब ये तमिलनाडू के तट से टकराती है तो वहाँ वर्षा कर देती है|
भारत में वर्षा के वितरण
भारत के पश्चिमी तथा उतरी-पूर्वी भागो में वार्षिक वर्षा 300 से.मी से अधिक होती है| पश्चिमी राजस्थान तथा इसके निकटवर्ती पंजाब, हरियाणा और गुजरात के क्षेत्रो में 50 से.मी से भी कम वार्षिक वर्षा होती है|
सह्याद्री के पूर्व में दक्कन के पठार के आंतरिक भागो में भी वर्षा कम होती है| कम वर्षा वाला तीसरा क्षेत्र कश्मीर में लेह के आसपास के प्रदेश है| बाकि देश के शेष भागो में साधारण वर्षा होती है|
हिमपात हिमालय के क्षेत्रो तक ही सीमित रहता है| मानसून की मनमानी के कारण वार्षिक वर्षा घटती बढती रहती है|
भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए
भारत की जलवायु को उतर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति और दक्षिण में हिन्द महासागर की उपस्थिति एवं भूमध्य रेखा से समीपता सबसे अधिक प्रभावित किया है| जल, एवं स्थल का असमान वितरण, वनस्पति आवरण महत्वपूर्ण कारक है| जो भारत की जलवायु को प्रभावित करके इसमें विविधता उत्पन्न करते है| इस विविधता पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव शीत तथा ग्रीष्मकाल में प्रभावित हो जाने वाली मानसून मानसून हवाओ का पड़ता है|
जलवायु को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक है|
धरातल की ऊंचाई
भारत में बहुत सारे पर्वत और पठार उपस्थित है| जो ग्रीष्मकाल में मैदानी भागो कि अपेक्षा कम तापमान मिलता है| क्योंकि वायुमंडल की उपरी परत का घनत्व निचली परतों की अपेक्षा कम रहता है| यही कारण है की विषुवत रेखा पर स्थित होते हुए भी इक्वेडर की राजधानी क्वीटो में चिरवसंत छाया रहता है| और अफ्रीका के केनिया-किलिमंजारो पहाड़ बर्फ से ढाका हुआ रहता है| पहाड़ी भाग में वाष्प भरे बदलो को अपनी ढाल के सहारे उपर उठाकर भारी वर्षा करने में सक्षम है|
वन
इसके आभाव में धरातल जल्दी गर्म हो जाता है| जो गर्मी के मौसम में शुष्क जलवायु मिलती है| घने पेड़-पौधे से ढाका हुआ धरती जल्दी गर्म नहीं हो पाती है और न ही सूखापन आता है| घने जंगल बादलों को अपनी और आकर्षित कर वर्षा करने को मजबूर करते है| जिससे जलवायु सम और नम हो जाती है|
पर्वतो की स्थिति
यदि किसी जगह पर पर्वत की दिशा चलने वाले पवन के समांतर हो तो वहाँ वर्षा नहीं हो पाती है| जैसे – राजस्थान में अरावली पहाड़ की दिशा अरबसागर से आनेवाली मानसून के समांतर है|
इसके विपरीत, यदि पर्वत की दिशा चलने वाले पवन के समकोण पर हो तो वहाँ भारी वर्षा हो सकती है| जैसे – मेघालय में
पर्वत के कारण यदि सम्मुख भाग वर्षा पता है| तो उसका विमुख भाग सुखा रह जाता है| जैसे – हिमालय का तिब्बत क्षेत्र
पवन के दिशा
गर्म मरुस्थलों से आने वाले पवन गर्म और ध्रुवो की और से चलने वाले पवन ठण्ड होते है| एवं समुद्री पवन आर्द्र और स्थलीय पवन शुष्क होता है| हमारे यहाँ गर्म हवा जो “लू” लेकर आती है| लेकिन समुद्र से आने वाली पूर्वी हवा ठण्ड होती है|
समुद्र की दुरी
गर्मी के मौसम में समुद्री हवा निकटतम क्षेत्रो में ठण्ड महसूस कराती है| लेकिन ठण्ड के मौसम में भायांकर सर्दी से भी बचाती है| अर्थात जलवायु को सम रखती है|
इसके विपरीत समुद्र से जितनी दूरी बढती है| वहाँ समुद्री हवा का प्रभाव कम होता जाता है| जिससे जलवायु विषम हो जाती है| इसलिए कोलकत्ता समुद्र के नजदीक होने के कारण जाड़ा काटने के लिए एक चादर ही काफी होती है| और उससे दूर पटना में एक कंबल की जरुरत पड़ती है| और उससे भी दूर दिल्ली में दो कंबलो के जरूरत पड़ती है|
भूमि की ढाल
भूमि की ढाल में दो बाते महत्वपूर्ण है, एक उसकी दिशा और दूसरी उसकी मात्रा| इसका मतलब ये होता है, यदि ढाल की दिशा सूर्य की और है तो तेज गर्मी मिलेगी| और ढाल सूर्य के उलटे दिशा में है तो कम गर्मी मिलेगी|
पहाड़ी भाग में जब रात का आकाश साफ रहता है| तो पृथ्वी से ताप विकिरण जल्दी हो जाता है| अर्थात ठण्डी हवा ढाल के सहारे घाटी में उतार आती है| तथा घटी की गर्म हवा ऊपर उठ जाती है, इससे वहाँ तापमान की विलोमता पायी जाती है| ऐसे प्रभाव ऊँचे पहाड़ों और उनकी घाटियों तक ही सीमित है| इसी कारण कैलिफोर्निया में घाटी के बजाय उच्च पर्वतीय ढाल पर होटल का कारोबार चलता है|
मिटटी
हमारे भारत देश में कुछ मिटटी ऐसे है जो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है| और कुछ मिटटी देर से गर्म होती है| ऐसे मिटटी जलवायु को तदनुसार प्रभावित करती है| रेतीला मैदान जल्द गर्म और ठण्ड भी हो जाते है| केवल मिटटी में देर तक नमी बनी रहती है| अतः वह देर से गर्म और देर से ठण्ड होती है|
संगमरमर में भी यही गुण है| जो गर्म इलाको में घर बनाने में इसका उपयोग होता है|
समुद्र और स्थल का वितरण
समुद्र धीरे-धीरे गर्म और ठण्डा होता है, और भूमि जल्दी गर्म होता है| समुद्र और स्थल की असामनता का स्पष्ट प्रभाव यह भी है कि समुद्र से चलने वाली पवन आर्द्र होती है| लेकिन स्थल से चलने वाली पवन शुष्क होती है| तटीय प्रदेश में जहाँ समुद्र की और से आने वाले पवन अधिक वर्षा करता है|
महासागरीय धाराएँ
इससे भी जलवायु पर अधिक प्रभाव पड़ता है| जो गर्म धाराएँ तटीय भाग का तापमान और वायु की आर्द्रता बढाती है और इसके विपरीत ठण्डी धाराएँ तापमान और आर्द्रता घटा देती है| कालाहारी मरुस्थल में सहारा की अपेक्षा ठण्डी जलवायु मिलने का प्रमुख कारण है|
अक्षांशीय स्थिति
अक्षांशो में स्थित किसी स्थान की जलवायु सूर्य की लंब किरणो के कारण गर्म होती है| जबकि उच्च अक्षांशो की और बढ़ने पर ठण्डी जलवायु मिलती है| क्योंकि वहाँ सूर्य की किरण तिरछी हो जाती है, जिससे सूर्यताप की मात्रा घटती जाती है| जिससे ध्रुव की बढ़ने पर वाष्पन की कमी से वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है|
भारत की जलवायु की विशेषताएं लिखिए
भारत की जलवायु का स्वरुप विषम है| कहा जाता है कि संसार में जलवायु की इतनी विषमताएँ नही मिलती जितनी अकेले भारत में मिलती है| मार्सडॉन के अनुसार विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पायी जाती है|
भारत की जलवायु की विषमताओ के कारण
भारत के जलवायु के विषमताओ के मुख्य करण कुछ इस प्रकार है|
दैनिक कारण – दिन और रात के तापमान में अंतर से जलवायु में विषमताएँ मिलती है| राजस्थान के भागो में मई महीने में दिन का तापमान 45 डिग्री से 50 डिग्री तक रहता है| परन्तु रात में यह घटकर 20 से 25 डिग्री तक हो जाता है| दूसरी और प्रायद्वीप भारत के तटीय भागो में सालोभर दैनिक तापमान में कोई विशेष अंतर नही आता है|
मासिक कारण – भारत की जलवायु के विषमता के कारण महीनो का चक्र है| उतरी भारत के मैदानी भागो में मई और जून में काफी तेज गर्मी पड़ती है| परन्तु कश्मीर के ऊँचे भागो में तापमान 0 डिग्री तक हो जाता है|
मौसमी कारण – ऋतू भी भारत के जलवायु को प्रभावित करती है| भारत में शीत, ग्रीष्म तथा वर्षा तीन ऋतू है| शीत ऋतू में उतर भारत में काफी ठण्ड बढ़ जाती है| वही दक्षिण भारत में गर्मी पड़ती है| पूर्वोतर भारत में जहाँ खूब वर्षा होती है| वहीँ राजस्थान में सुखा पड़ता है|
हिमालय की स्थिति – हिमालय पर्वत उतर में स्थित होने के कारण यह उतर ध्रुवीय ठण्डी वायु वायु राशियों के प्रभाव से हमे वंचित रखता है| और मानसूनी आर्द्र हवाओ को रोककर उतरी भारत के मैदानी भागो एवं पर्वतीय ढालो पर भारी वर्षा करती है|
भूमि का उच्चावच – भूमि का उच्चावच भी भारत की जलवायु को प्रभावित करती है| महावालेश्वर जो पश्चिमी घाट में श्रृंग पर स्थित है| जहा 625 सेंटीमीटर वर्षा होती है| और उसी के उतर-पूर्व में स्थित पुणे में उसके 10% वर्षा होती है|
तट रेखा – भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र तट रेखा से इतनी दुरी पर स्थित है कि समुद्र की जलवायु को मंद करने वाला कोई भी प्रभाव उसपर नही पड़ता है|
भारत के जलवायु का मानव जीवन पर प्रभाव
भारत का जलवायु मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है| जलवायु के प्रभाव के कारण ही यहाँ अनेक तरह की फसले पैदा की जाती है| यहाँ ऊँचे पर्वतीय भागो को छोड़कर सभी भागो में सालो भर कृषि कार्य एवं पशु पालन सम्भव है| यहाँ के जलवायु का प्रभाव फसल प्रारूप, सिंचाई व्यवस्था, पशुपालन, भारतीय अर्थतंत्र, राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन और देश की समृधि पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है| और देश का जन-जीवन भी इसमें प्रभावित रहता है| जनसँख्या का घनत्व एवं वितरण, लोगो के स्वास्थ, आचरण एवं व्यवहार, उधोग का स्थायीकारण, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापर, कार्य कुशलता संस्कृति एवं सामाजिक मूल्यों आदि पर जलवायु का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है|
भारत की जलवायु परिवर्तन
जलवायु की भिन्नता आर्थिक उपज में भिन्नता लाकर व्यापार को प्रभावित करती है| व्यापारिक मार्गो और व्यापारिक केंद्रों को भी जलवायु ने प्रभावित किया है| अत्यधिक ठंढी और अत्यधिक गर्म जलवायु मानव बसने के लिए उपयुक्त नहीं होती है| मानव की कार्यक्षमता उपयुक्त जलवायु में ही विकसित होती है|
जलवायु मानव के बसाव, मानव के किर्याकलाप और मानव के आर्थिक विकास में सहायक भी है, और बाधक भी| इसके प्रभाव से मानव अछुता नहीं रह सकता है| प्राकृतिक के साथ अनावशयक छेड़छड कर मानव जलवायु में परिवर्तन तो लाता है| लेकिन प्रकृति उसे कभी माफ़ नहीं करती है|
हडप्पा सभ्यता के विकास काल में जब अरावली क्षेत्र का वन-वैभव को नष्ट किया गया तो वहाँ की परिवर्तित जलवायु ने लोगो को ऐसी धुल चटाई कि वहाँ का सारा क्षेत्र वीरान हो गया|
विश्व की बढती जनसँख्या अतरिक्त भूमि की माँग कर रही है और प्राकृतिक के साथ हस्तक्षेप होने लगा है| उधोगो के विकास से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ चली है| जिसके चलते जलवायु-परिवर्तन के आसार नजर आने लगे है| हम इसके दुष्प्रभाव से बच नहीं सकते है|
निष्कर्स
हमने इस लेख के माध्यम से जलवायु जिला के बारे में बताने का प्रयास किया है.मै आशा करता हु कि आपलोग भली – भांति समझ गए होंगे. इस लेख में कहीं भी कोई शब्द छुट गया है. तो हमे कमेंट जरुर करे, अगर ये लेख जारा सा भी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों एवं सोशल मीडिया में जादा से जादा शेयर करे, धन्यवाद्